खेत की मिट्टी की सेहत के लिए रासायनिक से बेहतर है जैविक खाद
आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र विकासखण्ड जनपद पंचायत डौण्डी क्षेत्र के ग्राम पंचायत धोबनी ब में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधि सहित जनपद पंचायत के एसबीएम समन्वयक देवशरण यादव सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी शामिल थे।
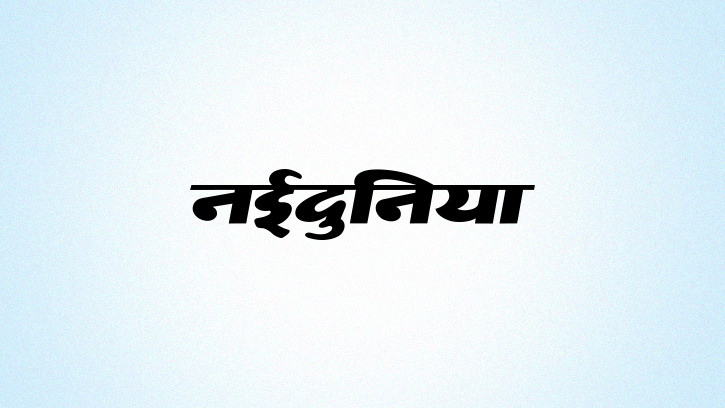
दल्लीराजहरा (नईदुनिया न्यूज)। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र विकासखण्ड जनपद पंचायत डौण्डी क्षेत्र के ग्राम पंचायत धोबनी ब में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधि सहित जनपद पंचायत के एसबीएम समन्वयक देवशरण यादव सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी शामिल थे। इस अवसर यादव ने कार्यशाला में ग्रामीणों को बताया कि मृदा स्वास्थ्य के लिए किसान रासायनिक उर्वरकों का सीमित प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि जैविक खादों का उपयोग बढ़ाएं। यह एक उत्तम जैविक खाद है। जो केचुओं से बनाई जाती है और इसे बहुत ही आसानी से तैयार किया जा सकता है। यह खाद कृषि के अवशेष पदार्थ शहर तथा रसोई के कूडे कचरे को पुनः उपयोगी पदार्थ में बदलने तथा प्रदूषण को कम करने की एक प्रभावशाली विधि है।
कौन से कृषि अवशेष प्रयोग हो सकते हैं
पुआल, भूसा, गन्नो की खोई, पत्तियां, खरपतवार, फूस, फसलों के डंठल, वायो गैस अवशेष तथा गोबर का प्रयोग कर यह तैयार की जा सकती है। इस खाद को तैयार करने में सब्जियों और फलों के छिलके जो फेंक दिए जाते हैं वे भी प्रयोग किये जा सकते हैं।
कौन से केंचुए बनाते हैं कंपोस्ट खाद
कंपोस्ट बनाने में सक्षम प्रजातियों में मुख्य रूप से आइनीसिया फोटिडा तथा यूड्िलस यूजिनी जिन्हें लाल केंचुआ भी कहते हैं। सबसे उत्तम हैं। यह खंड विकास कार्यालय से संपर्क कर मंगाए जा सकते हैं।
कैसे बनाएं वर्मी कंपोस्ट
किसी ऊंचे छायादार स्थान जैसे बगीचे आदि में 2 गुणा 1 मीटर का क्रमशः लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा बनाना होता है। विकल्प के रूप में इसी नाप का प्लास्टिक अथवा लकड़ी का डिब्बा प्रयोग किया जा सकता है। सबसे नीचे ईंट पत्थर की 11 सेमी की एक परत बनाने के बाद मुरूम या बालू की दूसरी तह बनाना होता है। इसके ऊपर 15 सेमी उपजाऊ मिट्टी की तह लगाकर पानी का हल्का छिड़काव कर दें। उसके बाद अधसड़ा गोबर डाल कर एक किलो प्रति गड्ढे की दर से उसमें केंचुआ छोड़ा जाता है। दें। उसके ऊपर पांच या 7 सेमी घरेलू कचरा या कृषि अवशेष डालने के 20-25 दिन तक आवश्यकतानुसार हल्का पानी छिड़क कर नमी बनाना होता है। प्रति सप्ताह इतनी ही कचरे की परत लगाते रहें जब तक कि पूरा गड्ढा भर न जाए। छह से सात सप्ताह में वर्मी कंपोस्ट बन कर तेैयार हो जाएगी।
वर्मी कम्पोस्ट के लाभ
पृथ्वी के भौतिक तथा जैविक गुणों में सुधार होता है। मृदा संरचना तथा वायु संरचना में सुधार होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं में वृृद्घि होती है। कूड़े-कचरे से फैलने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण होता है। इसी के साथ फलों, सब्जियों, खाद्यान्नाों की गुणवत्ता बढ़ती है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम कर मृदा स्वास्थ्य को सुरक्षित करने में सहायता मिलती है।